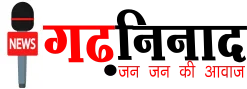“कोरोना काल में बदलती उत्तराखण्ड के गाँवों की सामाजिक-सांस्कृतिक तस्वीर’’

गढ़ निनाद न्यूज़ * 7 जून 2020
अल्मोड़ा: बड़ा अजीब संकट है। अपनी भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति के तमाम दावों के बावजूद मानव जितना असहाय आज दिख रहा है उतना पहले कभी नहीं दिखा। एक अतिसूक्ष्म जीव जिसे न सजीव कहा जा सकता है न निर्जीव ने ईश्वर की स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ कृति को आईना दिखाने का काम कर दिया है। यह संकट जिसे समझना वैश्विक समुदाय के लिए टेढ़ी खीर होता जा रहा है, ने मानव समुदाय में ही नहीं प्रकृति के प्रत्येक घटक में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया है। हम जानते हैं कि परिवर्तन कभी भी एक आयामी नहीं होता,इसके कई पहलू होते हैं।
अस्तु यहाँ पर मनुष्य समाज में, और वह भी विशेष कर उत्तराखण्ड के गाँवों की बदलती तस्वीर का जायजा लेना मकसद है, तो मैं जिक्र करुँगी सोशियल मीडिया पर वायरल हो रहीे वीडियोज का, जिनमें कहीं अपनों के आने का हर्ष है,तो कहीं हर्ष के साथ सालों की विरह- वेदना के गिले-शिकवे भी।
कुछ स्वारों, कुटुम्बियों के चेहरों पर जो फैलकर रहने-खाने की आदत सी हो गई थी, उसके सिमटने का भय है, तो कहीं इन प्रवासियों की हँसी उड़ाती वह तस्वीरें भी हैं जो पहले अपनी ईष्या को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते थे। वह आज कुटिल मुस्कान के साथ अब जैसे पूछना चाह रहे हों कि -’ अच्छा तब तो बड़े आदमी बनते थे। अब इन टूटे खण्डहरों और ढहती दीवारों के सहारे बंजर हो चुकी जमीनों के सहारे कैसे जीवन यापन करोगे? ऐसी ही अनगिनत भाव-भंगिमाओं को व्यक्त करता एक बुजुर्ग का वीडियो है, जिसमें वह अपनी धर्मपत्नी को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि-‘बहुत देशवाले बनते थे, अब इनको सिसौण (बिच्छू घास) के साग और मंडुवे (रागी) की रोटी के अतिरिक्त और कुछ खाने को मत देना। साथ ही बुजुर्गवार कह रहे हैं कि इन्हें अब घर आने की सूझी है, आये भी हैं तो बीमारी लेकर…”पहाड़ी में उनका यह अनवरत् प्रलाप वास्तव में अपने उन बेटे-बहू के प्रति नाराजगी को स्पष्टतया व्यक्त करता है, जो सुख के समय उन्हें छोड़कर चले गये और अब लौटे हैं जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है।”
एक दूसरा वीडियो है जिसमें एक बुजुर्ग चुपचाप बड़े ही शांत भाव से क्वारंटीन हुए अपने बहू और नाती-नातिन के लिए खाना रख रहे हैं। इसी वीडियो के बैकग्राउंड में बजते नरेन्द्र सिंह नेगी के गीत “छोया-ढुंग्यूं को पाणि पेजा…” इन बुजुर्ग की छवि को और अधिक दयनीय बना दे रहा है। ऐसे अनगिनत वीडियो के अतिरिक्त, अखबार में छपने वाले समाचारों से उत्तराखण्डियों की मानसिक उथल-पुथल को बखूबी समझा जा सकता है। कहीं दशकों पूर्व घर-द्वार से पलायन करने वाले व्यक्ति को घर में न घुसने देने की खबर है। तो कहीं माँ द्वारा गहने गिरवी रखकर पुत्र को वापिस लाने की कवायद का जिक्र।
प्रवासी उत्तराखंडियों की मानसिक स्थिति इनसे कहीं अधिक विकट है। कुछ परिवारजनों या ग्रामीणों से मिली अवहेलना से आहत हैं, तो कुछ गाँव वालों के स्नेह और सौहार्द को ही सच्ची पूँजी मानकर गाँवों में ही बसने का मन बना चुके हैं। फिर भी असमंजस, शक, शंका और अविश्वास यहाँ के विश्वस्त, दृढ़ तथा सहृदयी समाज पर हावी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग अभी भी सरकार से उम्मीद लगाये बैठे हैं कि मुख्यमंत्री इस रिवर्स पलायन से आबाद हो रहे गाँवों को पुनः खाली न होने देने के लिए न जाने कौन सी नीति या योजना की घोषणा कर दें।
कुछ लोग जिन्हें सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है, वे अपने बंजर खेतों में सब्जी उगाकर या अपनी टूटी गौशालाओं के पत्थर आदि ढूंढने लगे हैं इस उम्मीद से कि भविष्य में संभवतः यही उनके अर्थोपार्जन का सहारा बनेंगें।
उत्तराखण्ड के प्राकृतिक संसाधनों में पानी, जमीन, जंगल और बहुत कम मात्रा में खनिज हैं। समस्या यह है कि जमीन बहुत ही छोटी- छोटी जोतों में बंटी है। जोत का आकार इतना छोटा है कि कई बार तो हल-बैल के ठीक से घूमने की जगह भी खेत में नहीं होती। पानी पहाड़ी ढालों से बहकर,अपने साथ मिट्टी की उर्वरकता को भी ले जाता है। यही वजह रही थी कि राज्य निर्माण के बहुत पहले से ही चेक-डैम या चकबंदी जैसे विचार यहाँ के अनुभवी विचारकों के दिमाग में उपजे किंतु राजनीति एवं क्षुद्र स्वार्थों की भेंट चढ़ गये।
आज इन शब्दों को दोहराना बेवकूफी मात्र ही लगता है। जमीन जो यहाँ के लोगों के रोजगार का एक मात्र साधन है उस पर चारों ओर से संकट मंडरा रहे हैं- एक तो लम्बे समय से बंजर पड़ी रहने से उसकी उर्वरकता वैसे ही खत्म हो गई है। जहाँ थोड़ा बहुत लोग मेहनत द्वारा खेती कर भी रहे हैं उसको बंदरों व जंगली सुअरों ने तहस-नहस कर दिया है और बाकी रही सही भूमि बाहर से आये भू-माफियाओं की भेंट चढ़ गई है।
आज कोरोना संकट के इस दौर में यदि प्रवासी उत्तराखंडी आकर पुनः अपनी जमीन से अन्न उपजाकर अपना भरण-पोषण करना भी चाहें तो समस्याओं का अंबार इतना है कि इन परिस्थितियों में वह टिक पायेंगें मुश्किल लगता है। उत्तराखण्ड के लम्बे समय से ठहरे समाज में निश्चित रूप से हलचल बढ़ी है। गाँव जिनमें कुछ बूढ़े और लाचार लोग ही रह गये थे वे खुश हैं। उनकी खुशी दोहरी है- पहली इस अर्थ में कि अच्छा हुआ उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा, (भले ही यह तर्क अपने को भुलावे में रखकर खुश रहने के लिए गढ़ा गया हो) और दूसरे इस अर्थ में कि अब अगल-बगल टूटने की कगार पर खड़े खण्डहरनुमा मकानों में लोग आ बसे हैं, तो उनके जीवन में भी व्यस्तता बढ़ गयी है। समय के गुजरने का अहसास नहीं हो रहा है। गाँवों में पुरानी रौनक लौट आई है। गाँवों में सहभागिता और सामुदायिकता फिलहाल बढ़ती सी नजर आ रही है।
इस सामाजिक स्थिति का दूसरा पहलू यह भी है कि लोग डरे-सहमें भी हैं। डर दो तरह का है- एक तो आए हुए प्रवासियों से संक्रमित होने का, जो वहाँ रहने वालों को अधिक भयभीत कर रहा है, उन्हें घर लौटते लोग यमदूत से कम नजर नहीं आ रहे हैं। उनका यह डर अकारण भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर और दयनीय व्यवस्था किसी से छुपी भी नहीं है। भय आने वाले प्रवासियों के मन में भी है, सामाजिक तिरस्कार का और भविष्य के संकटों से जूझने का। इस दो-तरफे भय ने उत्तराखण्ड के गाँवों की सामाजिक समरसता और सौहार्दता को राजनीति से अधिक नुकसान बहुत थोड़े से समय में पहुँचा दिया है। पहले जब भी प्रवासी लोग आते थे, तो ऐसे अवसरों पर आते थे कि सब कुछ खुशनुमा लगता था। शादी, धार्मिक पूजा या गर्मियों की छुट्टियों में यदा-कदा आने वाले इन प्रवासियों के लिए गाँव वर्ष भर की थकान मिटाने वाले पिकनिक स्पाॅट थे किंतु अब स्थितियाँ बदली हुई हैं। न आने वालों को मालूम है कि वह कब लौटेंगे, लौटेंगे भी या नहीं?और न आतिथेयों को पता है कि इस स्थिति में कब तक रहना है। यहाँ यह भी विचारणीय पहलू है कि मध्यमवर्गीय वे परिवार जो ठीक-ठाक आर्थिक स्थिति में हैं, वे घर नहीं लौटे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर ही हर आपदा की तरह यह आपदा भी भारी पड़ी है।
उत्तराखण्ड में पर्यटन, धार्मिक पूजा पाठ और परिवहन पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने वालों की संख्या अधिक है, और इन लोगों की कमर पहले ही टूट गई है। केदारनाथ आपदा के पश्चात् पिछले दो सालों में सब कुछ पुनः पटरी पर लौट रहा था कि कोरोना ने फिर से सब-कुछ तहस-नहस कर दिया है।
उत्तराखण्ड की संस्कृति को भी इन परिस्थितियों से तगड़ा झटका
बिखोत में लगने वाले बड़े-बड़े मेलों से जो शुरुआत होती है और मई के महीने तक थौल- धारों में जो मेले लगते थे, थड़िया-चैंफला खेलने की जो बची खुची रस्म थी वह भी कोरोना की भेंट चढ़ गईं हैं। इस बार कहीं भी मेलों का आयोजन नहीं हुआ है। अप्रैल में विवाहिता बेटियों और बहनों को भेजे जाने वाले ’चैती-कलेऊ’ या ’भिटौली’ का रूप मनीआॅर्डर में तब्दील हो गया। भिटौली या चैती कलेऊ के बहाने ही सही एक दिन मायके वालों को अपने सारे काम-काजों को एक तरफ रखकर बेटी या बहन के घर जाना ही पड़ता था।
गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करने वाले दादा- दादी और नाना-नानी के घर जाकर उनके पोपले मुँह पर भी मुस्कान ला देते थे और स्वयं स्कूल की मारामारी से दूर प्रकृति की गोद में दो-चार दिन ही सही अपने सहज बचपन को जीते थे। लाॅकडाउन में ऑनलाइन टीचिंग में सर खपा रहे हैं।
अब तो वह बच्चे भी जो कभी स्कूल नहीं जाना चाहता था, स्कूल खुलने की मन्नतें माँगने लगा है। यह स्थिति कमोवेश सभी जगहों की है, किंतु पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ आदमी स्वच्छंदता से जीने का आदी होता है, घर की चाहरदीवारी से अधिक खुले में जीवन जीता है उसके लिए लाॅकडाउन एक नया अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसमें मनुष्य के मनोमस्तिष्क को बुरी तरह प्रभावित किया है।
तत्कालिक प्रभाव तो खबरों के माध्यम से सामने आ ही जा रहे हैं, किंतु इनसे कहीं अधिक प्रभाव उन संवेदनशील मनुष्यों पर मनोवैज्ञानिक रूप से पड़ा है जो अपने आपको खुलकर किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् “ईश्वर की मृत्यु” की घोषणा करने वाले मनुष्य का दिमाग अब किस करवट बैठेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
डाॅ0 अमिता प्रकाश
रा बा इं कॉलेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा